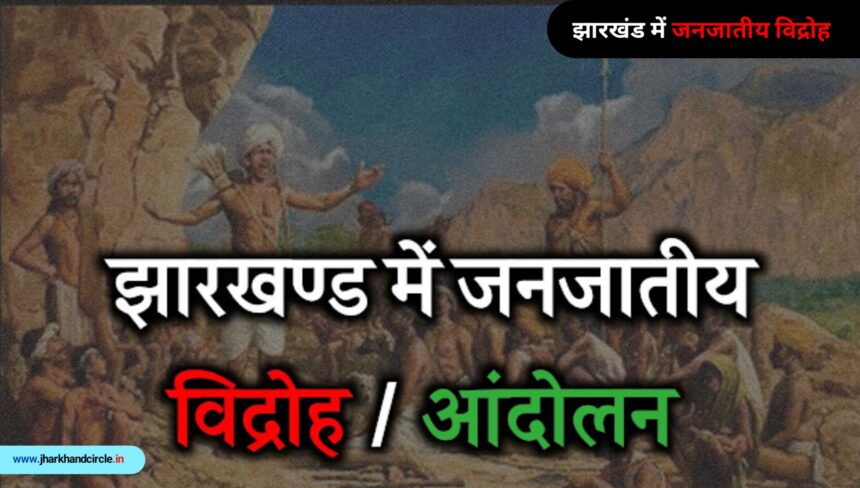जनजातीय विद्रोहों [ Tribal movements ( revolts ) in Jharkhand ] के पीछे कई गहन और महत्वपूर्ण कारण थे। इनमें मुख्यतः तीन प्रमुख कारण सम्मिलित थे। पहला कारण था राजनीतिक: उपनिवेशी शासन और उनकी नीतियों ने जनजातियों के पारंपरिक स्वायत्तता और अधिकारों को छीन लिया, जिससे उनमें गहरा असंतोष पनपने लगा। दूसरा कारण था आर्थिक: अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों, ज़मींदारी प्रथा और वन कानूनों ने जनजातियों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया, उनकी जीविका के साधनों पर गहरा संकट आ गया। तीसरा कारण था सामाजिक-सांस्कृतिक : उपनिवेशी शासन ने जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं पर आक्रमण किया, जिससे उनकी सामाजिक संरचना और जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इन सब कारणों ने मिलकर जनजातीय समाज को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया।
झारखण्ड में जनजातीय विद्रोह – राजनीतिक कारण
झारखण्ड में विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारण कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित थे। सबसे पहले, आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार जमाने का प्रयास एक प्रमुख कारण था। ब्रिटिश शासन और अन्य बाहरी शक्तियों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा करने और उनके संसाधनों का दोहन करने की कोशिश की, जिससे स्थानीय आदिवासी जनसंख्या में गहरा असंतोष पैदा हुआ।
दूसरे, आदिवासी शासकों को नियंत्रित करने का निरंतर प्रयास भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ब्रिटिश सरकार और उनके अधीनस्थ अधिकारी आदिवासी नेताओं को अपने अधीन करने और उनकी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करते थे, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया।
तीसरे, आदिवासी स्वायत्ता पर नियंत्रण की कोशिश भी विद्रोह को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। आदिवासी समुदाय अपनी स्वायत्तता और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्षरत थे, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप और नियंत्रण के प्रयासों ने उन्हें विद्रोह करने के लिए मजबूर किया।
चौथे, ब्रिटिश शासन द्वारा थोपे गए नियमों और कानूनों ने आदिवासियों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप किया। ये नियम और कानून आदिवासी समाज की परंपराओं और उनके जीवन जीने के तरीके के विपरीत थे, जिससे असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ी।
पाँचवे, ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण भी एक गंभीर मुद्दा था। शोषण की इस प्रक्रिया में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया, उनके संसाधनों का दोहन किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिससे विद्रोह की आग और भड़क उठी।
अंत में, जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना भी विद्रोह के पीछे एक प्रमुख कारण था। जमींदार अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए आदिवासियों को उकसाते थे, जिससे उनका असंतोष और बढ़ जाता था और वे विद्रोह के मार्ग पर चल पड़ते थे।
इन सभी कारणों ने मिलकर झारखण्ड में एक व्यापक विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, जिससे क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में गहरा प्रभाव पड़ा।
झारखण्ड में जनजातीय विद्रोह – आर्थिक कारण
जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण: हमारे देश के आदिवासी समुदायों को लंबे समय से जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषित किया जाता रहा है। ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन उच्च ब्याज दरों के जाल में फंसकर अपनी संपत्ति और जमीनें खो देते हैं। इस शोषण से आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है।
अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू करना : अंग्रेजी शासन के दौरान, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई, जिसने किसानों और आदिवासियों पर भारी बोझ डाल दिया। इस व्यवस्था के तहत किसानों को निश्चित मात्रा में कर देना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई, और उनका जीवन यापन कठिन हो गया।
अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव : लगातार आने वाले अकालों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया। फसलों की बर्बादी से किसानों की आय पर भारी असर पड़ा, जिससे उनका जीवन यापन कठिन हो गया। अकाल की पुनरावृत्ति ने खाद्य संकट को बढ़ाया और गरीबी को और गहरा कर दिया।
कृषि संबंधी अन्य समस्याएँ : किसानों को कृषि से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बीज, उर्वरक, और सिंचाई की कमी। इसके अलावा, आधुनिक तकनीक और ज्ञान की कमी के कारण उनकी कृषि उत्पादन क्षमता भी सीमित रहती है। इन सभी समस्याओं के चलते उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता और वे गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं।
वन कानूनों द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण : वन कानूनों के लागू होने से आदिवासी समुदायों के पारंपरिक निर्वाह साधनों पर प्रतिबंध लग गया। वे वन उत्पादों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब उन्हें जंगलों में प्रवेश करने और संसाधनों का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और उनका जीवन यापन और भी कठिन हो गया है।
इन सभी आर्थिक कारणों ने मिलकर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया है, जिससे उनका जीवन यापन अत्यंत कठिन हो गया है।
झारखण्ड में जनजातीय विद्रोह – सामाजिक-सांस्कृतिक कारण
झारखण्ड में जनजातीय विद्रोह के पीछे कई गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हुए हैं, जो आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और उनके परंपराओं पर आधारित हैं।
पहला प्रमुख कारण है जनजातीय परंपराओं में बाहरी हस्तक्षेप। आदिवासियों की अपनी विशिष्ट परंपराएं और रीति-रिवाज होते हैं, जिनमें हस्तक्षेप उन्हें अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए खतरा महसूस कराता है। बाहरी लोग, जिन्हें आमतौर पर ‘दिकु’ कहा जाता है, जब इन परंपराओं में दखल देते हैं, तो यह आदिवासियों के लिए असहनीय हो जाता है और विद्रोह का रूप ले लेता है।
दूसरा कारण है दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन दृष्टि से देखना। आदिवासी समाज का एक समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा है, जिसे अक्सर बाहरी लोग समझ नहीं पाते और उन्हें हीन मानते हैं। यह भेदभाव और अनादर आदिवासियों के अंदर गुस्सा और असंतोष भर देता है, जो समय के साथ विद्रोह का कारण बनता है।
तीसरा महत्वपूर्ण कारण है इसाई धर्म के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयास। मिशनरियों द्वारा इसाई धर्म का प्रसार आदिवासी समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित करता है। उनकी पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं खतरे में पड़ जाती हैं, जिससे वे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विद्रोह करने पर मजबूर हो जाते हैं।
इन सभी कारणों ने मिलकर झारखण्ड में जनजातीय विद्रोह की आग को हवा दी है, जो एक समृद्ध और स्वतंत्र आदिवासी संस्कृति की रक्षा के संघर्ष का प्रतीक है।
आइये अब पढ़ते है ( Tribal Revolts / Movements in jharkhand ) झारखण्ड में जनजातीय विद्रोह के बारे में –
ढाल विद्रोह ( Dhaal Vidroh ) : 1767-1777
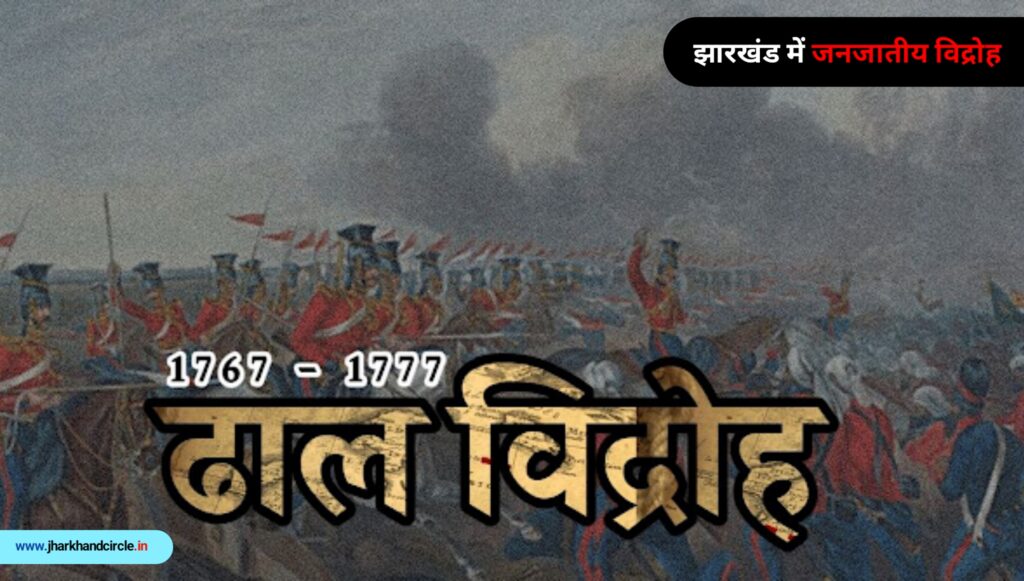
ढाल विद्रोह झारखण्ड प्रदेश में अंग्रेजों के विरूद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है ‘ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह । अंग्रेजों ने ‘ सिंहभूम की दीवानी ‘ प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया जिसके प्रतिक्रियास्वरूप वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ई. में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ जो 1777 ई. तक (10 वर्ष) चला। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था।इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, परन्तु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। 1777 ई. में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। ढालभूम का राजा बनाये जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को अधिकतम 4000 रूपये कर देना स्वीकार किया गया। 1780 ई. में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रूपये कर दिया गया। झारखण्ड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था।
चुआर विद्रोह ( Chuaar Vidroh ) : 1769-1805

अंग्रेज जंगलमहल के भूमिजों को चुआर/चुआड़ (नीची जाति के लोग) कहते थे जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ा। सामान्यत: चुआर लोग पशु-पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती व वनोत्पादों के व्यापार द्वारा अपना भरण-पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहां सिपाही (पाइक) के रूप में कार्यरत थे। अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को ब्रिकी करने, जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरूद्ध यह विद्रोह किया गया। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम एवं पंचेत राज्य में हुआ। घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदायों के समर्थन कारण इस विद्रोह ने व्यपाक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह में भूमिज जनजाति ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर (1769-71 तक); मंगल सिंह (1782-84 तक), लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह (1798-99 तक) ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाड़भूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था –
‘अपना गाँव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज‘।
ले. गुडयार, कैप्टन फोर्स एवं मेजर क्रॉफ्ड को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएँ देने का निर्णय लिया। 6 मार्च, 1800 ई. को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी-घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुर्नस्थापित किया गया जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। साथ ही पइकों की जब्त भूमि की वापसी व जमींदारों की भूमि की अवैध निलामी पर रोक का भी निर्णय लिया गया। 1805 ई. में जंगलमहल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुयी।
चेरो विद्रोह ( Chero Vidroh ) : 1770-1819
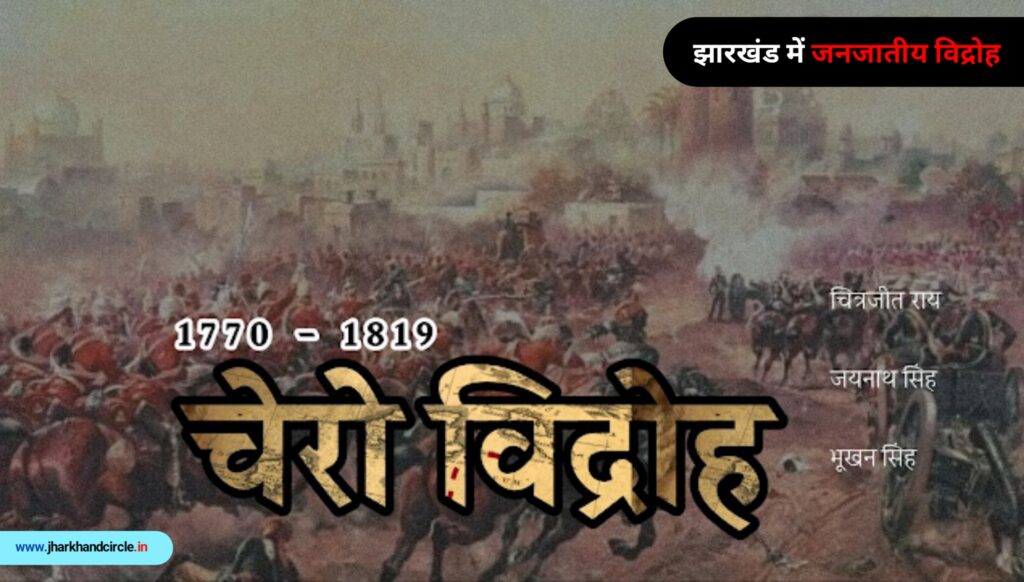
चेरो विद्रोह ( प्रथम चरण ) : 1770-71
उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह कर दिया इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को सर्मथन प्रदान करना था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया तथा 1 जुलाई, 1771 ई. को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया।
चेरो विद्रोह ( द्वितीय चरण ) : 1800-19
इस विद्रोह का दूसरा चरण सन् 1800 में भुखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 ई. में कर्नल जोंस के नेतृत्व में राजा भुखन सिंह को गिरफ्तार करके फाँसी दे दी गयी, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। 1809 ई. में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। 1813 ई. में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। 1815 ई. में अंग्रेजों ने नीलाम किये गए राज्य को देव के राजा धनश्याम सिंह से बेच दिया जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। साथ ही धनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया।
उपरोक्त घटनाओं के परिणामस्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 में अंग्रेजों के विरूद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। इसका विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने रफसेज को नियुक्त किया जिसने जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1819 ई. में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की निलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा धनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 ई. में चेरों ने धनश्याम सिंह व अंग्रेजों के विरूद्ध पुनः विद्रोह कर दिया।
भोगता विद्रोह ( Bhogta Vidroh ) : 1770-1771
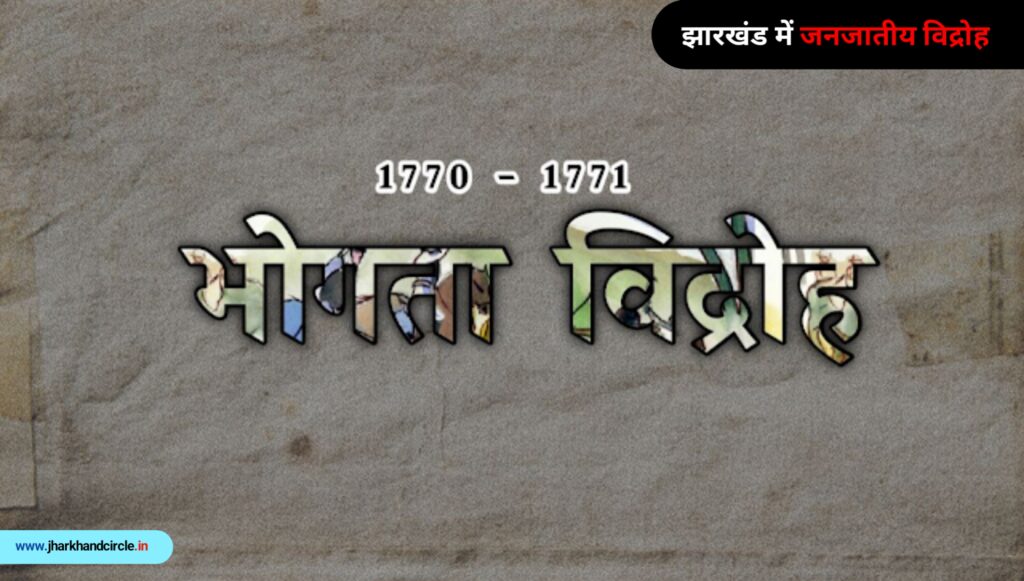
यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानान्तर प्रारंभ हुआ तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोगता (चित्रजीत राय का दीवान) ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परन्तु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोगता एवं चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया।जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया।
घटवाल विद्रोह ( Ghatwaal Vidroh ) : 1772-1773

घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। परिणामतः अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किये गये इस दुर्व्यवहार के विरूद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर, 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैमक का विरोध करने लगे। परन्तु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होनें मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किये ही समाप्त हो गया। इस विद्रोह में छै व चंपा के राजा ने भी मुकुद सिंह का साथ दिया था। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद से कभी शांत नहीं रहा तथा वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा। परन्तु उसने इन्कार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप एकरमेन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगाँव भेज दिया गया।
रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे जिसे देखते हुए उपकलेक्टर जी. डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाय और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाय।
पहाड़िया विद्रोह ( Pahadiya Vidroh ) : 1772-1782

पहाड़िया जनजाति की तीन उपजातियाँ हैं–
1. माल पहाड़िया 2. सौरिया पहाड़िया 3. कुमारभाग पहाड़िया
सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़िया विद्रोह चार चरणों ( 1772, 1778, 1779, 1781-82 ) में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न-भिन्न थे।
1772 ई. में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना आहड़ी ने किया। 1778 ई. में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरूद्ध संगठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गयी थी। 1779 ई. में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1781-82 ई. में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह ‘दामिन-ए-कोह’ के विरोध में किया गया था। 1790-1810 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया तथा 1824 ई. में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को ‘दामिन-ए-कोह’ का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया।
तमाड़ विद्रोह ( Tamad Vidroh ) : 1782-1821

इस विद्रोह का प्रारंभ मुण्डा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरूद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। यह अंग्रेजों के विरूद्ध सबसे लम्बा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था।’ यह विद्रोह छः चरणों में संचालित हुआ।
तमाड़ विद्रोह ( प्रथम चरण ) : 1782-83
सन् 1782 में रामगढ़, पंचेत तथा वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया। साथ ही इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। सन् 1783 के अंत में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किये जाने के बाद यह विद्रोह अगले पांच वर्षों के लिए शांत हो गया।
तमाड़ विद्रोह ( द्वितीय चरण ) : 1789
पांच वर्षो बाद 1789 ई. में मुण्डाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इंकार कर दिया जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन होगन को भेजा गया जो असफल रहा।पुनः अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कुपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कुपर के प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्रोह अगले चार वर्षों तक शांत रहा।
तमाड़ विद्रोह ( तृतीय चरण ) : 1794-98
1794 ई. में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 ई. में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 1796 ई. में राहे के राजा नरेन्द्र शाही द्वारा अंग्रेजों का साथ दिये जाने के कारण सोनाहतू गाँव में आदिवासियों द्वारा नरेन्द्र शाही का विरोध किया गया। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता रामशाही मुंडा ने भी इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। विद्रोहियों द्वारा रिश्तेदार की हत्या किये जाने के बाद राहे के राजा नरेन्द्र शाही फरार हो गये। 1798 ई. में कैप्टेन लिमण्ड द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टेन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया।
तमाड़ विद्रोह ( चतुर्थ चरण ) : 1807-08
1807 ई. में दुखन मानकी के नेतृत्व में मुण्डा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 1808 ई. में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार किये जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया।
तमाड़ विद्रोह ( पांचवां चरण ) : 1810-12
1810 ई. में नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच. ओडोनेल को भेजा गया जिसने 1812 ई. में नावागढ़ पर हमला कर दिया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया जिसके बाद यह विद्रोह मंद पड़ गया।
तमाड़ विद्रोह ( छठा चरण ) : 1819-21
1819 ई. में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा जिसके सबसे प्रमुख नेता रूदन मुण्डा तथा कुंटा मुण्डा थे। इसके अतिरिक्त इसमें दौलतराय मुण्डा, मंगलराय मुण्डा, गाजीराय मुण्डा, मुचिराय मुण्डा, भदरा मुण्डा, झुलकारी मुण्डा, टेपा मानकी, शंकर मानकी, चंदन सिंह, घुन्सा सरदार आदि ने भी भाग लिया। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंगेज अधिकारी ई. रफसेज ने ए. जे. कोलविन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रूदन मुण्डा व कुंटा मुण्डा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गये। जुलाई, 1820 में रूदन मुण्डा तथा मार्च, 1821 में कुंटा मुण्डा के गिरफ्तार होने के साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया।
तिलका आंदोलन ( Tilka Andolan ) : 1783-1785
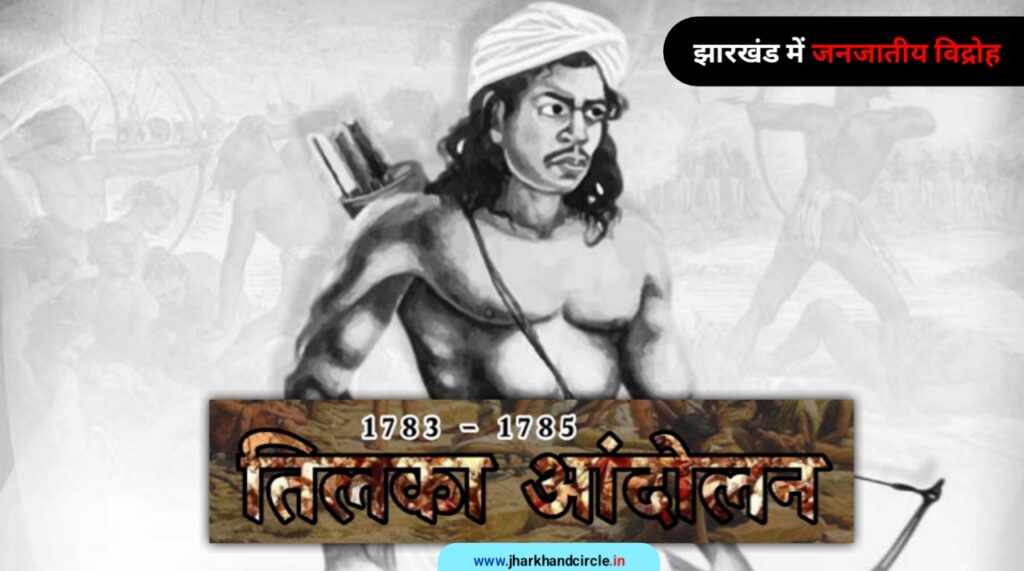
तिलका आंदोलन की शुरूआत 1783 ई. में तिलका माँझी और उनके समर्थकों द्वारा की गयी थी। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया।इसका प्रमुख उद्देश्य था-
◑ आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना।
◑ अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ना ।
◑ सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना ।
इस आंदोलन का प्रमुख केन्द्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। झारखण्ड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ।तिलका माँझी उर्फ जाबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार-प्रसार हेतु ‘साल के पत्तों’ का प्रयोग किया। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी, 1784 को तिलका माँझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड* की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने तिलका माँझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेजों द्वारा तिलका माँझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका माँझी ने छापामारी युद्ध (गुरिल्ला युद्ध) का प्रयोग किया। छापामार युद्ध की शुरूआत तिलका माँझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गयी थी। संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका माँझी कमजोर पड़ गया तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जउराह ने तिलका माँझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। 1785 ई. में अंग्रेजों द्वारा तिलका माँझी को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलका माँझी को 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ से फाँसी पर लटका दिया गया। इस स्थान को उनकी की याद में बाबा तिलका माँझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका माँझी हैं।’ ( नोट:- तिलका माँझी अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे तथा इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। )
मुण्डा विद्रोह ( Munda Vidroh ) : 1793-1832
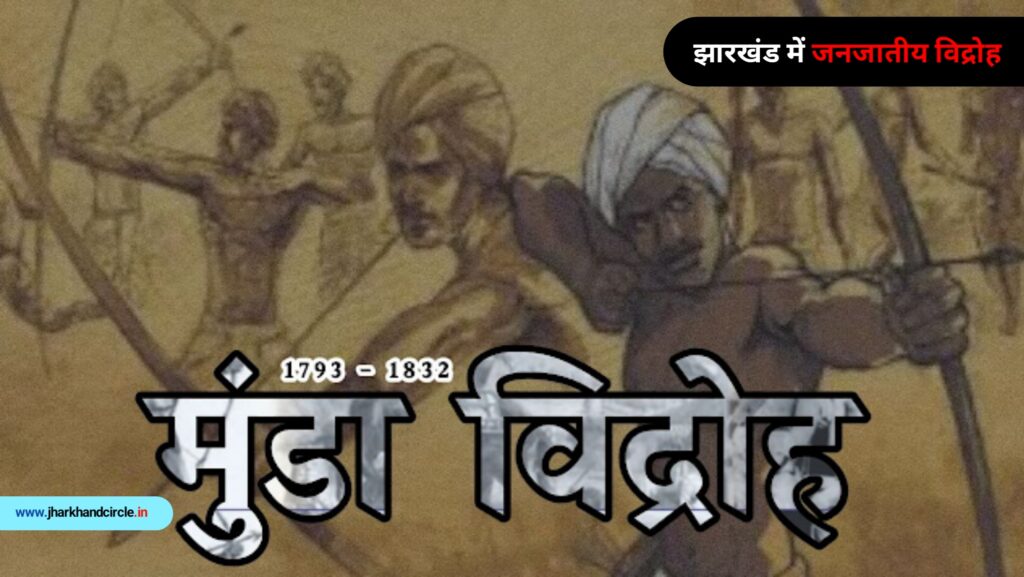
झारखण्ड के इतिहास में मुण्डाओं के विद्रोहों की संख्या अनेक है, किन्तु बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में संचालित ‘मुण्डा उलगुलान’ इनमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप का था। बिरसा मुण्डा के आंदोलन के पूर्व मुण्डाओं द्वारा अलग-अलग उद्देश्यों से निम्न विद्रोहों का संचालन किया गया:-
1793 ई. का बुण्डू एवं राहे का मुण्डा विद्रोह
1793 ई. का मुण्डा विद्रोह वास्तव में 1789 ई. में विष्णु मानकी * के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था जिसका विस्तार बुण्डू और राहे में हुआ। इस विद्रोह का कारण बुण्डू और राहे के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता को अस्वीकार करना था। इस विद्रोह का दमन मेजर फॉलर द्वारा किया गया।
1796 ई. का सिल्ली एवं राहे का मुण्डा विद्रोह
1796 ई. में सिल्ली एवं राहे के मुण्डा विद्रोह को रामशाही मुण्डा और ठाकुरदास मुण्डा ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह के दौरान मुण्डाओं ने नरेन्द्र शाही तथा कुँवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया।
1807 ई. का तमाड़ का मुण्डा विद्रोह
1807 ई. में तमाड़ में मुण्डा विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बन्दोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था।
1819-20 ई. का पलामू का मुण्डा विद्रोह
पलामू में 1819-20 में भूकन सिंह के नेतृत्व में मुण्डा विद्रोह का संचालन हुआ।
1832 ई. में बुद्ध भगत का मुण्डा विद्रोह
1832 ई. के मुण्डा विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत ने किया।
हो विद्रोह ( Ho Vidroh ) : 1820-1821
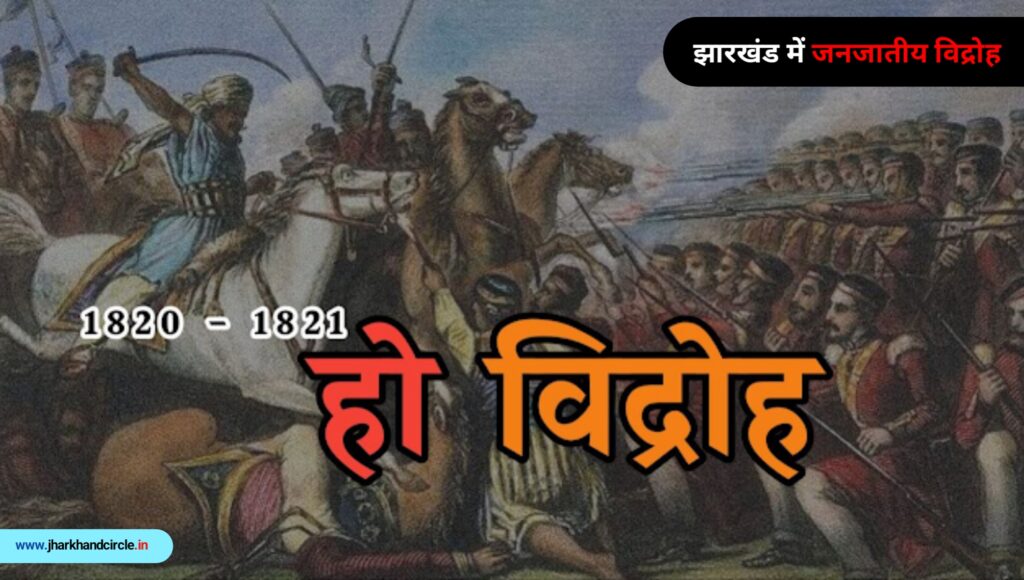
‘हो देशम’ ( हो लोगों का निवास स्थान ) पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। पोरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था तथा वह हो जनजाति से नियमित कर की अपेक्षा करता था। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय व लड़ाका स्वभाव के थे तथा ये राजा को नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ई. में मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। जिसके परिणामस्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहाट के राजा व अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरूद्ध एक युद्ध हुआ जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। इस दमन के बाद ‘हो देशम’ के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लागों ने कर देने से मना कर दिया व उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। विवश होकर पोरहाट के राजा ने पुनः मेजर रफसेज से सहायता मांगी। रफसेज ने 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा जिसका एक माह तक हो लागों ने सामाना किया। अंग्रेजों के विरूद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना क्षीण देखकर हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने तथा राजा व जमींदारों को प्रति हल आठ आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बाद में पुन: हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 के कोल विद्रोह में ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।
कोल विद्रोह ( Kol Vidroh ) : 1831-1832
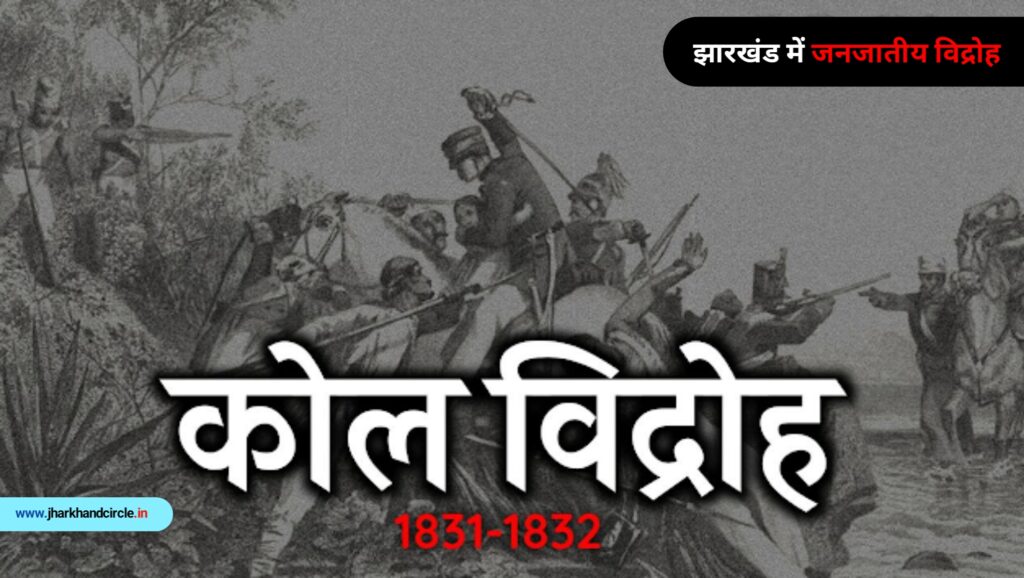
कोल विद्रोह झारखण्ड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। अतः झारखण्ड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोहों में इसका विशेष स्थान है। इस विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखत थे–
◑ लगान की ऊँची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति।
◑ अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना।
◑ जमींदारों व जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न ।
◑दिकुओं (अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर-आदिवासी कर्मचारी), ठेकेदारों व व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण।
◑ अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर (उदाहरणस्वरूप 1824 में हड़िया पर लगाया गया ‘पतचुई’ नामक कर ) ।
◑ विभिन्न मामलों के निपटारे हेतु आदिवासियों के परंपरागत ‘पड़हा पंचायत व्यवस्था’ के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना।
इस विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी के बारह गाँवों की जमीन छीनकर सिक्खों को दे दी गई तथा सिक्खों ने सिंगरई की दो बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। इसी प्रकार सिंहभूम के बंदगाँव में जफर अली नामक मुसलमान ने सुर्गा मुण्डा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप सिंदराय मानकी व सुर्गा मुण्डा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गाँवों पर हमला कर दिया जो सिंदराय से छीन लिये गये थे। इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गाँव में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसकी व्यवस्था बंदगाँव के बिंदराय मानकी ने की थी। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गाँव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके दस आदमियों को मार डाला। यह विद्रोह 1831 ई. में प्रारंभ होने के अत्यंत तीव्रता से छोटानागपुर खास, पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र तक प्रसारित हो गया।
इस विद्रोह को मुण्डा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण एस. आर. टिकेल ने इन्हें ‘लरका कोल’ से संबोधित किया। हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिह्न के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्ध भगत (सिल्ली निवासी) अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गये। बुद्ध भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया।
विभिन्न हथियारों व सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेना के विरूद्ध केवल तीर-धनुष से लैस विद्रोहियों ने दो महीने तक डटकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बदले में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उन्हें 313 रूपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। 1832 ई. में सिंदराय मानकी तथा सुर्गा मुण्डा (बंदगाँव, सिंहभूम निवासी) ने आत्मसमर्पण कर दिया जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह के बाद छोटानागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ई. का रेगुलेशन-III लागू किया गया। साथ ही जंगलमहल जिला को समाप्त कर नन-रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसे बाद में दक्षिण-पश्चिम सीमा एजेंसी का नाम दिया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गयी तथा इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। इस विद्रोह के बाद मुण्डा-मानकी शासन प्रणाली को भी वित्तीय व न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गये।
भूमिज विद्रोह ( Bhumiz Vidroh ) : 1832-1833
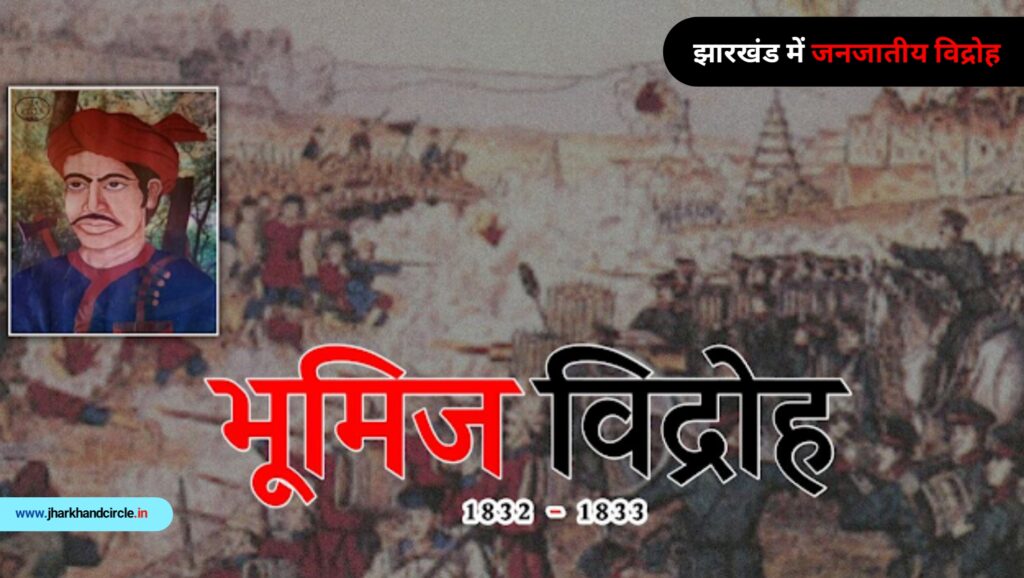
भूमिजों द्वारा जंगलमहल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा चुआड़ कहा जाता था। भूमिजों द्वारा संचालित ढालभूम के इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। अतः इस विद्रोह को ‘गंगा नारायण का हंगामा’ की संज्ञा दी जाती है | आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता बिंदराय मानकी का भी समर्थन प्राप्त हुआ।
1798 ई. में अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा कर गलत तरीके से गंगा गोविंद सिंह को बाड़भूम का राजा नियुक्ति किया। पूर्व में भी अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा करके लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया था व लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया था जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी। नवनियुक्त राजा ने जनता पर विभिन्न अनैतिक कर आरोपित कर दिये, जिससे जनता में राजा के प्रति असंतोष फैलने लगा। इसके अतिरिक्त बाड़भूम के दीवान माधव सिंह ( राजा गंगा गोविंद सिंह का सौतेला भाई) ने चालाकी से अपने चचेरे भाई गंगा नारायण (लक्ष्मण सिंह का पुत्र) को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी। गंगा नारायण ने अपनी जागीर प्राप्ति हेतु कंपनी शासन से बार-बार आग्रह किया जिसकी हर बार अनदेखी की गयी।
इस प्रकार विद्रोह का प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियमों की अनदेखी, जनता पर अनैतिक कर, दिकुओं द्वारा जनता का शोषण व गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार था। गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया तथा दीवान माधव सिंह की 26 अप्रैल, 1832 ई. को हत्या कर दी जिसके परिणामस्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। इसके बाद गंगा नारायण ने घटवालों की एक बड़ी सेना के साथ संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाड़भूम पर चढ़ाई कर दी। इस अभियान में सूरा नायक, बुली महतो, गर्दी सरदार आदि गंगा नारायण के प्रमुख सहयोगी थे।
इस अभियान के दौरान गंगा नारायण ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया तथा मई, 1832 में रसेल के नेतृत्ववाली तथा नवंबर, 1832 में ब्रेडन व ट्रिमर के नेतृत्ववाली अंग्रेजी सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया। गंगा नारायण द्वारा अंग्रेजों पर इस सफल हमले के बाद नवंबर, 1832 में ही अंग्रेज अधिकारी डेन्ट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण व उनके साथियों के विरूद्ध अभियान चलाया तथा इनके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ गया। गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला गया तथा कोल लड़ाकों के साथ मिलकर उसने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर धावा बोल दिया। 7 फरवरी, 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरूद्ध लड़ते समय गंगा नारायण की मृत्यु हो गयी जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनामस्वरूप 5,000 रूपये मिले। गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत हो गया। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम व वीरभूम क्षेत्र में था।’ इस विद्रोह के बाद जंगलमहल क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। 1833 ई. के रगुलेशन-XIII के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया तथा जंगलमहल जिला को समाप्त कर दिया गया।
संथाल विद्रोह ( Santhal Vidroh ) : 1855-1856
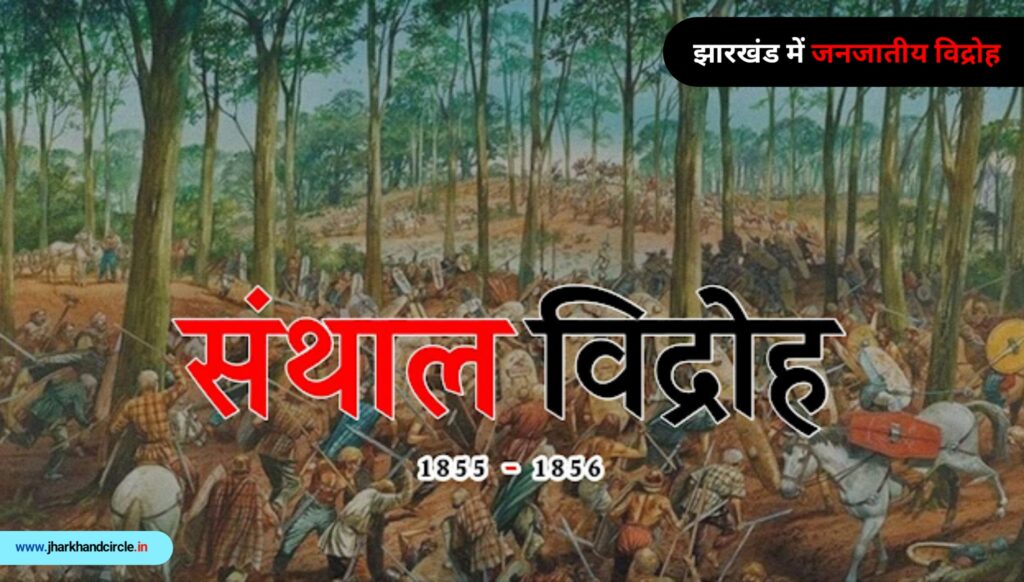
इस विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू-कान्हू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्रांति/बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। काल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को सिद्धू-कान्हू , चांद-भैरव तथा फूलो-झानों ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई-बहन थे। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ई. तक संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होनें संथाल परगना के क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। 1815-30 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण प्रारंभ हो गया। जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ब्रिटिश सरकार ( पुलिस व न्याय व्यवस्था ) द्वारा संथालों का शोषण आदि इसके विभिन्न स्वरूप थे। इसके अतिरिक्त भागलपुर से वर्द्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया गया तथा बेगार करने से मना करने पर इन्हें शारीरिक दण्ड दिया जाने लगा। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ई. में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर-आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दिधी थाने के दारोगा महेशलाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया तथा जेल में विजय माँझी नामक एक संथाल की मौत हो गयी। एक संथाल ने आक्रामक रूख दिखाते हुए दारोगा की हत्या कर दी जिसका सभी संथालों ने समर्थन किया।
इसके बाद 30 जून, 1855 को भोगनाडीह गाँव में लगभग 400 गाँवों के 6,000 से अधिक आदिवासियों एक सभा की जिसमें ‘अपना देश, अपना राज’ का नारा दिया गया तथा विद्रोह का बिगुल फूंका गया। ( 30 जून को ‘हूल दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। ) इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। इस सभा में सिद्धू-कान्हू ने यह घोषणा की कि ‘भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो।’ इसके साथ ही उन्होनें भविष्यवाणी की कि ‘अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे।’ इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ तथा यह धीरे-धीरे हजारीबाग, वीरभूम एवं छोटानागपुर आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई माँझी एवं अर्जुन माँझी ने तथा वीरभूम में गोरा माँझी ने किया। इस विद्रोह के दौरान ‘जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश’ नामक नारा भी दिया गया।
इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई, 1855 को जनरल लायड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गयी, परन्तु सेना का मेजर बारो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। 16-17 सितंबर, 1855 को सुंदरा व रामा माँझी तथा मुचिया कोमनाजेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया। करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर, 1855 को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रूपये का इनाम घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्ण कदम उठाया तथा दिसंबर, 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर, 1855 को फाँसी की सजा दे दी गयी।इसके बाद चाँद व भैरव को बड़हैत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। फरवरी, 1856 में कान्हु भी पकड़ा गया तथा उसे 23 फरवरी, 1856 को अपने ही भोगनाडीह गाँव के ठाकुरबाड़ी परिसर में फाँसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लफ्टिनेंट थामसन एवं लफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।इस विद्रोह में 50 हजार से अधिक संथाली पुरुष-महिलाओं ने भागीदारी की जिसमें से 15 हजार से अधिक लोग मारे गये।
इस विद्रोह का प्रसार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग (नेतृत्वकर्त्ता – जुबाई माँझी व अर्जुन माँझी) व वीरभूम (नेतृत्वकर्त्ता – गोरा माँझी) क्षेत्र में भी था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर, 1856 को नान- रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाजत नहीं थी।संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एशली एडेन था। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट-37 के अनुसार ‘दामिन-ए-कोह’ का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नयी सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक चार उपजिले बनाए गये। 1856 ई. में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जार्ज यूल की सहायता से ‘यूल रूल’ नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गयी। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गयी। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे ‘खूनी विद्रोह’ भी कहा जाता है।
सरदारी आंदोलन ( Sardari Aandolan ) : 1858-1895
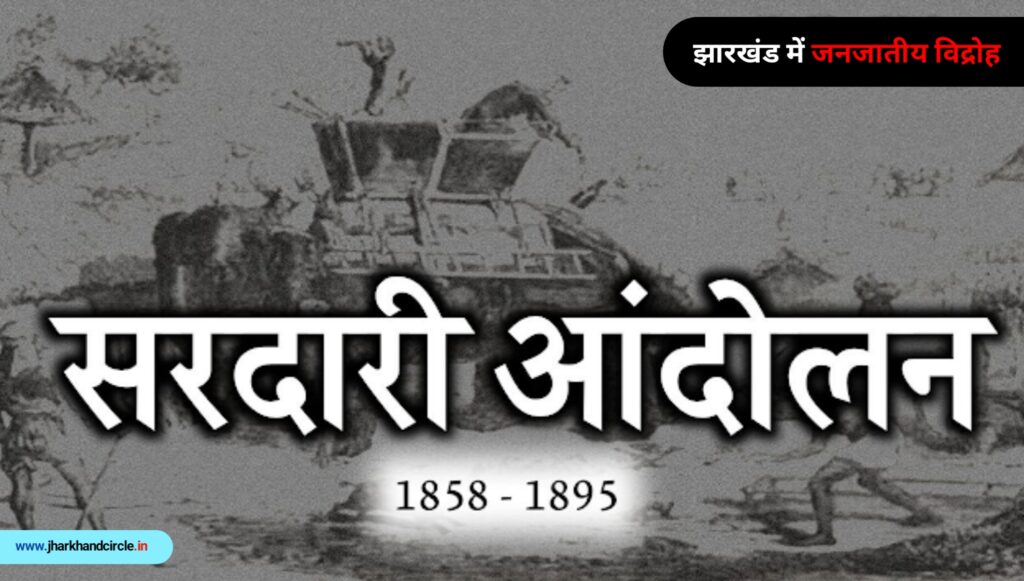
इस आंदोलन को ‘मुल्की व मिल्की (मातृभूमि व जमीन) का आंदोलन’ भी कहा जाता है। 1831-32 के कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बगानों में काम करने हेतु चले आए थे। काम करने के बाद जब वे अपने गाँव लौटे तो पाया कि उनकी जमीनों को दूसरे लोगों ने हड़प लिया है तथा वे जमीन वापस करने से इनकार कर रहे थे। इसी हड़पे गये जमीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से किराये में वृद्धि करना भी इस आंदोलन के कारणों में शामिल था। इस आंदोलन में कोल सरदारों को उराँव व मुण्डा जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग-अलग उद्देश्यों के आधार पर इस आंदोलन के तीन चरण परिलक्षित होते हैं – प्रथम चरण भूमि आंदोलन के रूप में (1858-81 ई. तक), द्वितीय चरण पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में (1881-90 ई. तक) तथा तीसरा चरण राजनैतिक आंदोलन के रूप में (1890-95 ई. तक) ।
सरदारी आंदोलन ( प्रथम चरण ) : 1858-81 ई.
आंदोलन का यह चरण अपनी हड़पी गयी भूमि को वापस पाने से संबंधित था। अतः इसे भूमि आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन छोटानागपुर खास से शुरू हुआ तथा दोइसा, खुखरा, सोनपुर और वसिया इसके प्रमुख केन्द्र थे।इस आंदोलन का तेजी से प्रसार होने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा भुईंहरी (उराँवों की जमीन) काश्त के सर्वेक्षण हेतु लाल लोकनाथ को जिम्मेदारी प्रदान की गयी। इस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने भूमि की पुनः वापसी हेतु 1869 ई. में छोटानागपुर टेन्यूर्स एक्ट लागू किया। इस कानून में पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनी गयी भुईंहरी व मंझियस भूमि (जमींदारों की भूमि) को वापस लौटाने का प्रावधान था। इस कानून को लागू करते हुए 1869-80 तक भूमि वापसी की प्रक्रिया संचालित रही जिससे कई गांवों के रैयतों को अपनी जमीनें वापस मिल गयीं। परंतु राजहंस (राजाओं की जमीन), कोड़कर (सदानों की जमीन) व खूँटकट्टी (मुण्डाओं की जमीन) की बन्दोबस्ती का प्रावधान इस कानून में नहीं होने के कारण सरदारी लोग पूर्णत: संतुष्ट नहीं हो सके।
सरदारी आंदोलन ( द्वितीय चरण ) : 1881-90 ई.
आंदोलन के इस चरण का मूल उद्देश्य अपने पारंपरिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना था। अतः इसे पुनर्स्थापना आंदोलन कहा जाता है।
सरदारी आंदोलन ( तृतीय चरण ) : 1890-95 ई.
इस चरण में आंदोलन का स्वरूप राजनैतिक हो गया। आदिवासियों ने अपनी हड़पी गयी जमीनें वापस पाने हेतु विभिन्न इसाई मिशनरियों, वकीलों आदि से बार-बार सहायता मांगी। परंतु सहायता के नाम पर इन्हें हर बार झूठा आश्वासन दिया गया। परिणामतः आदिवासी इनसे चिढ़ने लगे। ब्रिटिश शासन द्वारा दिकुओं व जमींदारों का साथ देने के कारण आदिवासियों का अंग्रेजी सरकार पर भी भरोसा नहीं रहा। परिणामतः आदिवासियों ने 1892 ई. में मिशनरियों व ठेकेदारों को मारने का निर्णय लिया। परंतु मजबूत नेतृत्व के अभाव में वे इस कार्य में सफल नहीं हो सके। बाद में बिरसा मुण्डा का सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय बिरसा आंदोलन में हो गया।
साफाहोड़ आंदोलन ( Safahod Aandolan ) : 1870

साफाहोड़ का अर्थ होता है – ‘ सिंगबोंगा के प्रति समर्पण।’ इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को ‘राम-नाम’ का मंत्र दिया तथा मांस-मदिरा के सेवन से रोका। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में ‘देशोद्धारक दल’ की स्थापना की। इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भतू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। बंगम माँझी * भी इस विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था।
खरवार आंदोलन ( Kharwar Aandolan ) : 1874

खरवार, संथालों की ही एक उपजाति है तथा ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण-युग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु यह एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। इस आंदोलन की भागीरथ माँझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में शुरूआत 1874 ई. में संथाल परगना क्षेत्र में हुई। भागीरथ माँझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा गाँव में हुआ था।
भागीरथ माँझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इसे ‘भागीरथ माँझी का आंदोलन’ भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान भागीरथ माँझी ने स्वयं को बौंसी गाँव का राजा घोषित किया तथा ब्रिटिश सरकार/जमींदारों को कर नहीं देने की अपील करते हुए खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु निम्न विचारों का प्रचार-प्रसार किया गया
◑ सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी-देवता की उपासना का परित्याग।
◑ सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाचने-गाने का परित्याग।
◑ सिद्धू-कान्हू (संथाल विद्रोह के नेता) के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता।
◑ संथाल विरोधियों का प्रतिकार तथा उपपंथो की संख्या को बारह तक सीमित करना।
◑ उपासकों का साफाहोड़ (समर्पण के साथ उपासना करने वाले), भिक्षुक/बाबाजिया (उदासीनता के साथ उपासना करने वाले) तथा मेल बरागर (बेमन से उपासना करने वाले) में वर्गीकरण।
इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ माँझी एव उनके सहयोगी ज्ञान परगनैत को गिरफ्तार कर लिया। नवंबर, 1877 में दोनों को रिहा कर दिया गया जिसके बाद यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुबु बाबा ने किया। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसांई के नेतृत्व में 1881 ई. की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया। परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दुविधा गोसांई की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया।
बिरसा आंदोलन ( Birsa Aandolan ) : 1895-1900

इस आंदोलन को ‘मुण्डा उलगुलान’ भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है – विद्रोह हलचल। 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलनों में यह सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 ई. में बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यद्यपि यह आंदोलन राजनीतिक (स्वतंत्र मुण्डा राज की स्थापना), धार्मिक (इसाई मुण्डाओं को वापस अपने धर्म में लाना) एवं आर्थिक (मुण्डाओं की जमीन पर पुनः अधिकार स्थापित करना) उद्देश्यों से भी प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे-
◑ खूँटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या ।
◑ मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन।
◑ मुण्डाओं की समस्याओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता।
◑ 1894 ई. का छोटानागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह साधनों पर संकट ।
1895 ई. में बिरसा मुण्डा ने ‘सिंगबोंगा धर्म’ का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया तथा विभिन्न बोंगाओं (देवताओं) के स्थान पर सिंगबोंगा की अराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुण्डा ने स्वयं को ‘सिंगबोंगा का दूत’ घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य सिंगबोंगा देवता की अराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूँटी था। इस विद्रोह के समय राँची का उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड था। इस आंदोलन में गया मुण्डा (सेनापति), दोन्का मुण्डा (राजनीतिक शाखा प्रमुख) तथा सोमा मुण्डा (धार्मिक-सामाजिक शाखा प्रमुख) ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तारित किया। बिरसा मुण्डा के आंदोलन में गया मुण्डा की पत्नी मनकी मुण्डा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मुण्डा आंदोलन के समय ‘कटोंग बाबा कटोंग’ नामक गीत प्रमुख था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान ‘अबुआ राज एटेजाना, महारानी राज टुंडू (अब मुण्डा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी का राज समाप्त हो गया है)’ का ऐलान भी किया। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुण्डा को दो बार डोरंडा कारागार (राँची) में बंदी बनाकर रखा गया:-
1. पहली बार – 24.08.1895 से 30.11.1897 तक
अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा गिरफ्तारी) – ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तारी।
2. दूसरी बार – 03.02.1900 से 09.06.1900 तक
पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद 30 नवंबर, 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुण्डा को रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के पश्चात् बिरसा मुण्डा ने पुनः लोगों को संगठित करना शुरू किया तथा गाँव-गाँव को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 24 दिसंबर, 1899 को बिरसा मुण्डा ने डुंबारू मुरू में आयोजित एक सभा में अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया तथा 25 दिसंबर, 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया।
इस बार बिरसा मुण्डा ने ठेकेदारों, हाकिमों, जागीरदारों व इसाईयों को मारने की अपील की। बिरसा मुण्डा ने घोषणा की कि ‘दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा’।इसके बाद इनके अनुयायियों ने आक्रमकता दिखाते हुए गिरिजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। देश के विभिन्न समाचार-पत्रों ने बिरसा मुण्डा के आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचारों का प्रकाशन किया। इसमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का ‘बंगाली’ नामक समाचार पत्र प्रमुख था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ई. में डोम्बारी पहाड़ी (सैल रकब पहाड़ी) पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस व स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जांलियावाला बाग की तर्ज भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। बिरसा मुण्डा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रूपये का ईनाम घोषित किया था। बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 मार्च,1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय बिरसा मुण्डा को गिरफ्तारी कर लिया गया। 9 जून, 1900 ई. को राँची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुण्डा की मृत्यु हो गयी। इस आंदोलन में शामिल 300 मुण्डा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया जिसमें से 3 को फाँसी दी गयी एवं 44 को आजीवन कारावास की सजा दी गयी। इसके अलावा 47 लोगों को कड़ी सजा दी गयी, जिसमें गया मुण्डा की पत्नी मनकी मुण्डा को 2 वर्ष जेल की सजा सुनायी गयी। इसी आंदोलन के परिणामस्वरूप 1902 ई. में गुमला को एवं 1903 ई. में खूँटी को अलग अनुमंडल बनाया गया व नये न्यायालय की स्थापना की गई।इसके अतिरिक्त राँची जिले का सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गयी। इसी विद्रोह के प्रभावस्वरूप 11 नवंबर, 1908 ई. को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) पारित किया गया। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था (खूँटकट्टी) को पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ-साथ लगान की दरों में कटौती की गयी। बिरसा मुण्डा के आंदोलन अपने मूल उद्देश्य (मुण्डा राज की स्थापना) को पाने में तो असफल रहा, परंतु इसने पृथक झारखण्ड के निर्माण हेतु आधारशिला तैयार कर दी।
ताना / टाना भगत आंदोलन ( Tana Bhagat Aandolan ) : 1914
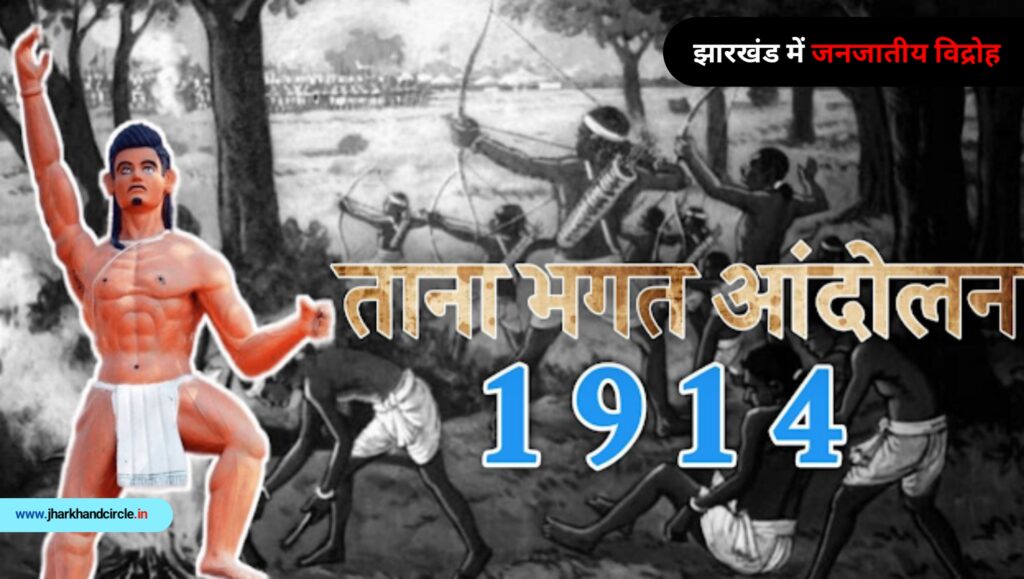
ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल, 1914 ई. में गुमला से हुआ। इस आंदोलन को बिरसा मुण्डा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस-मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, विशुनपुर में भिखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरूख धरम आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुरूख या उराँव जनजाति का मूल धर्म है।
1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके एक वर्ष की सजा दे दी गयी। परंतु बाद में उसे शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के दो माह बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गयी। इनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गयी प्रताड़ना थी। मांडर में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्त्ता शिबू भगत द्वारा टाना भगतों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके परिणामस्वरूप टाना भगत दो भागों में विभक्त हो गये। इनमें मांस खाने वाले वर्ग को जुलाहा भगत’ तथा शाकाहारी वर्ग को ‘अरूवा भगत’ (अरवा चावल खाने वाले) का नाम दिया गया। धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ यह आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1916 ई. के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार राँची के साथ-साथ पलामू तक फैल गया। टाना भगतों ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग रखी। राजा ने इन मांगो को अस्वीकृत कर दिया जिसके कारण टाना भगतों व राजा के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस आंदोलन का विस्तार सरगुजा तक हो गया था।
1919 ई. में छोटानागपुर प्रमण्डल में टाना भगत आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देविया भगत, सिंहा भगत, माया भगत व सुकरा भगत को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी गयी, परंतु आंदोलन जारी रहा। दिसंबर, 1919 ई. में तुरिया भगत एवं जीतु भगत ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णत: अहिंसक था तथा ताना भगतों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गाँधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 ई. के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ताना भगतों ने ‘सिद्धू भगत’ के नेतृत्व में भाग लिया था। इस दौरान टाना भगतों ने शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी आदि द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत किया।
महात्मा गाँधी से प्रभावित होकर टाना भगतों ने चरख व खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार टाना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। ताना भगतों नेकांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन व 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। यह विशुद्ध गाँधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। 1930 ई. में सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था जिससे प्रभावित होकर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गाँधी को 400 रूपये उपहारस्वरूप प्रदान किए थे। 1948 ई. में ‘राँची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद्’ अधिनियम पारित किया गया था।
हरिबाबा आंदोलन ( Haribaba Aandolan ) : 1931

यह आंदोलन हरिबाबा उर्फ दुका हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। इस आंदोलन में बारकेला क्षेत्र के भूतागाँव निवासी सिंगराई हो, भड़ाहातू क्षेत्र के बामिया हो तथा गाड़िया क्षेत्र के हरि, दुला व बिरजो हो ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। यह आंदोलन भी गांधीजी के विचारों से प्रभावित था।
:::
झारखंड में जनजातीय विद्रोह (आंदोलन) की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि जब किसी समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान पर संकट आता है, तो वह समाज अपनी भावना की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है। युवाओं ने अपनी रक्षा के लिए अपना अधिकार और पहचान कायम की है। उनके संघर्ष की गाथा हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज की सच्ची प्रगति संभव है, जब हम उनके धर्म, संस्कृति और सिद्धांतों का सम्मान करते हैं।
झारखंड का इतिहास इन विद्रोहों से प्रेरणा पाता है और हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे लिए एक संदेश है कि हम सामूहिक समूह एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां हर समुदाय को लाभ, सम्मान और न्याय मिले।
झारखंड के अधिकार का यह संघर्ष केवल उनकी भूमि, सामर्थ्य और अधिकार के लिए नहीं था, बल्कि यह उनकी पहचान और गौरव की रक्षा का भी संघर्ष था। हमें उनके इस संघर्ष को समझने और सराहने की जरूरत है, ताकि हम उनके योगदान को सही मायनों में पहचान सकें और एक सामुदायिक समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकें।
मैं, आकाशदीप कुमार, आशा करता हूं कि इस ब्लॉग में आपको झारखंड में जनजातीय विद्रोह की गहराई को समझने में मदद मिलेगी। झारखंड से जुड़ी और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए jharhandcircle.in के साथ।
धन्यवाद।